आदिवासी युगों से आजादी पसंद समाज रहा है
आदिवासी समाज युगों से आजादी पसंद समाज रहा है। वह न तो किसी राज्य शक्ति के अधीन कभी रहा था, न ही कोई राज्य शक्ति उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों का नियंत्रक था। बिरसा मुंडा, सिदो, कानू , चांद, भैरव, टंट्याभील, भीमा नायक, अल्लूरी सीताराम राजू, तिलका माँझी, बुधु भगत, बिंदराय मानकी, तेलंगा खड़िया, टंट्या भील आदि सैकड़ों महापुरूषों का आंदोलन इसी आजादी पसंद समाज का आंदोलन और संघर्ष था। आदिवासी समाज प्राकृतिक जीवन जीने की कला का हमेशा कायल रहा है। इसीलिए स्वाभाव की प्रकृति से भी वह अक्खड़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप वह किसी मानव निर्मित दर्शन को न मान कर प्राकृतिक को ही सब कुछ मानता है और पारंपारिक रूप से वह प्राकृतिक पूजक बन गया है। स्वभाव से वह कभी भी किसी आप्रकृतिक विचारधारा, सिद्धांत के साथ जीवन जीना नहीं सीखा।
हर मानव स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समूह उस पर अपना बचपन से ही नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास जारी रखते हैं, क्योंकि अधिसंख्यक मानव ही उनकी सत्ता और शक्ति का स्रोत होता है। उत्पादन, वितरण और खपत पर चालाक मानव समूह का ही नियंत्रण होता है । इसीलिए मानवीय समूहों के विशेष क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण करके ही सभी शक्तियॉं अपनी सत्ता को बनाए रखती है।
लेकिन आदिवासी समाज को किसी पराए सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक सिद्धांत या नियमों के तहत बंधने का कोई भी प्रयास पसंद नहीं था। आम आदिवासी दर्शन में समाज को जो कुछ भी प्राप्त था, वह सब कुछ प्राकृतिक का दिया हुआ नैसर्गिक देन था। इसी प्राकृतिक विचारधारा से ओतप्रोत वह न तो जमींदारी प्रथा और न ही अंग्रेजो के द्वारा मालगुजारी प्रथा को स्वभाविक ढंग से स्वीकार किया। वह जमींदारों के बेगारी प्रथा से भी बहुत क्रुद्ध था। भूमि, खेत खलिहान, जंगल, जल, नदी, पहाड, जीवन जीने की स्वाभाविक मर्जी आदि को वह प्राकृतिक (ईश्वर) का दिया हुआ मानता रहा है और कोई राजा, कोई साम्राज्य अथवा किसी शासकीय सत्ता को कभी भी अपना मालिक नहीं माना। इन्हीं विशेषताओं के कारण आदिवासी समाज को एक स्वच्छंद स्वतंत्रता पसंद जीवन का स्वामी माना गया है। बाहरी शक्तियों चाह कर भी प्रत्यक्ष रूप से अपनी जीवन दर्शन को उन पर उनकी मर्जी के बगैर थोपने में नाकामयाब रही।
सत्रहवीं और अठारहवीं सदी में भारत के सभी आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों की राजसत्ता को आदिवासियों ने हथियारबंद चुनौती दिया था। जमींदारों और अन्य ब्रिट्श एजेंटों के माध्यम से अंग्रेज अपनी व्यवस्था, जीवन दर्शन को उन पर लाद रहे थे। आदिवासी समाज को आयातित धार्मिक दर्शनों को नियोजित ढंग से दिमाग में डाल रहे थे। अत्यंत शुरूआत में आदिवासी समाज ने इसे बहुत गुरूत्व नहीं दिया, लेकिन बाद में देश भर के आदिवासी समाजों ने इसका तीब्र विरोध किया गया।
AMAZON ONLINE
Click here to check the prices and get up to 80% OFF
1772-80 के पहाडिया विद्रोह, 1780-85 का तिलका माझी के नेतृत्प में संताल विद्रोह, 1795-1800 के तमाड और मुण्डा विद्रोह, 1798 के वीरभूम, बांकुडा के चौर विद्रोह, विद्रोह, 1798-99 के मानभूम में भुमिज विद्रोह, 1800-02 में तमाड के दुखन मानकी के नेतृत्व में मुण्डा विद्रोह, 1819-20 में भुखन सिंह मुण्डा के नेतृत्व में हुए मुण्डा विद्रोह, 1832-33 में भागीरथी, दबाई गोसाईं और पटेल सिंह के नेतृत्व में हुए खेरवार विद्रोह, 1833-34 में वीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भुमिज विद्रोह, 1855-60 के संथाल विद्रोह इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में अल्लूरी सीताराम राजू (1922) और कोमुरम भीमा (1928-40) तथा अन्य की अगुवाई में आदिवासी समाज अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के लिए अलग से संघर्ष कर रहा था।
उन्नीसवीं सदी के दौरान एक पैसे का मोल बहुत था और आदिवासी विद्रोह से अंग्रेज कितने हैरान परेशान या डरे हुए थे कि संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू और उसके भाई कान्हू को पकडने के लिए अंग्रेजों ने दस हजार रूपये इनाम घोषित किया था। 1856-57 में बुधुबीर उरॉंव विद्रोह, 1874-99 को भगवान बिरसा मुण्डा के नेतृत्व में उठे उलगुलान आंदोलन, 1914 के टाना भगत आंदोलन, 1919 में डुवार्स के तेभागा आंदोलन आदि में लाखों आदिवासियों ने अपनी स्वतंत्रता और स्वराज्य को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया। वे अंग्रेजों और उनके एजेंटों के वजूद को मिटाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए थे।
जमींदारी प्रथा और प्रशासन के माध्यम से आदिवासी अंचलों और समाजों को नियंत्रित करने का प्रयास आदिवासी समाज की सार्वभौमिकता के लिए एक गहरा धक्का था। वे हैरान थे कि ये कैसे लोग और सिस्टम हैं जो हम आदिवासियों को, हमारी अस्मिता और समाज को अपने नियंत्रणाधीन रखने का सजो सामान समझते हैं। ये लोग किस तरह और कैसे प्राकृतिक या ईश्वर का स्थान लेने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी समाज में युगों से समता और समानता की भावना और मूल्य गहरे मन:स्थिति में पैठ चुकी थी और वे अपने को न तो किसी से उँचा या श्रेष्ठ समझते थे न ही किसी को अपने से कमतर।
दो मानव के बीच प्राकृतिक रूप से असमानता की भावना समाज में दूर-दूर तक नहीं थी। समाज में धर्म, संस्कृति, भाषा, खेती पद्धति, शादी-विवाह, पर्व-त्यौहारों, नृत्य-गीत, हॅसी-मजाक या शिकार जैसे सामूहिक कार्यो में भी कभी उँच नीच और भेदभाव का कोई परंपरा का विकास नहीं हो पाया। लेकिन पक्षपातीय भावनाओं और कमजोरों के शोषण पर आधारित सिद्धांत के द्वारा समाज को नियंत्रित करने की बाहरी दुर्गुणों को समाज में थोपने की कोशिश करने वालों के प्रति समाज हमेशा प्रतिरोध किया और प्रतिहिंसक हो उठने तक अपनी अस्वीकार्यता को प्रकट किया है।
अपने जीवन पद्धति, स्वशासन और स्वतंत्रता के प्रति अत्यंत संवेदनशील आदिवासियों के हिंसक प्रतिरोधी आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए शिड्युल्ड डिस्ट्रिक (The Scheduled District Act of 1874 (Act XIV of 1874) बनाया। शिड्युल्ड डिस्ट्रिक के लिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था के तहत सेंट्रल और प्रोविंसियल लेजिस्लेटिव को कानून बनाने का हक नहीं था। लेकिन गवर्नर इन कौंसिल को हक था कि वह प्रोविंसियल कौसिल के द्वारा पारित किसी भी कानून को शिड्युल्ड डिस्ट्रिाक में लागू करने का आदेश दे सकता था किन्तु गवर्नर जनरल के द्वारा उक्त कानून के किसी भाग के अपवाद और संशोधन (subject to such exceptions or modifications as the Governor thinks fit) की अनुमति होने के बाद Montague-Chelmsford Reforms treated में इन्हीं क्षेत्रों को Backward Tracts कहा गया और भारत सरकार अधिनियम 1919 को इन क्षेत्रों में लागू करने से रोका गया ।
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत में बढ रहे असंतोष को कुंद करने के लिए बनाए गए सुधारवादी कानूनों को इन क्षेत्रों में लागू नहीं किया । लेकिन कुछ समय उपरांत इन क्षेत्रों को दो भागों में बॉट कर कुछ भागों में आंशिक रूप से सुधारवादी कानूनों को लागू किया गया । इन्हीं दो भागों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत साइमन कमिशन के सुझाव के अनुसार Excluded Areas and Partially Excluded Areas कहा गया और प्रस्ताव दिया गया कि इन क्षेत्रों का प्रशासन प्रांतीय सरकार से लेकर भारत सरकार के हाथों में दिया जाए। इन क्षेत्रों में गवर्नर जनरल की विशेष अनुमति के सिवा कोई भी साधारण कानून अपवादों और संशोघन के शर्तो के सिवाय आदिवासियों के लिए लागू नहीं होता था । इन क्षेत्रों में किसी भी कानून को तब तक लागू नहीं किया जा सकता था, जब तक कि स्वयं गवर्नर जनरल अपनी विवेकाधीन शर्तो के सहित अनुमति न दें। इन्हीं क्षेत्रों में ही देश की आजादी के बाद पॉचवी अनुसूची के प्रावधानों को लागू किया गया । उत्तर पूर्वी राज्यों को छोडकर देश के अन्य हिस्सों में बसने वाली अनुसूचित जनजाति के सांस्कृतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, राजनैतिक, आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान की धारा 244 (1) के उपबंध बनाए गए।
शिड्युल्ड डिस्ट्रिक बना कर आदिवासियों को साधारण कानून से मुक्त रखने का प्रमुख कारण था कि प्रगतिशील समाजों पर शासन करने के लिए बनाए गए कानून ओर उसके नियम काफी दुरूह, जटिल और विभिन्न प्रकार से व्याख्या पर आधारित होते हैं। उन कानूनों और नियमों के सहारे कानून की बारीक जानकारी रखने वाले समाज या समूह उन्हें अपने शोषण का माध्यम बना सकते हैं। शिड्युल्ड डिस्ट्रिक बना कर एक ओर उन्हें कानूनी दॉव पेंच और मुकादमेबाजी के वातावरण से बचाया गया, दूसरी ओर उन्हें इसके माध्यम से स्थानीय शासन स्वयं चलाने के लिए ऑटोनोमस दिया गया।
Gazette of India, 1881,Pt.I p.74 के अनुसार The Scheduled Districts Act, 1874 (14 of 1874), के द्वारा जलपाईपाई जिला के पश्चिम जलपाईगुडी और पश्चिमी डुवार्स को शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक के रूप में घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि रंगपुर जिला के उत्तरी भाग और पश्चिम डुवार्स (वर्तमान डुवार्स अंचल) (असम के कुछ जिले कभी पुर्वी डुवार्स के रूप में जाना जाता था) को मिला कर 1869 में जलपाईगुडी जिले का गठन किया गया था। तब तक डुवार्स तराई में अनेक चाय बगान बन चुके थे और यहॉं छोटानागपुर, संथाल परगाना के मजदूर स्थायी रूप से बस गए थे। उल्लेखनीय है कि शिड्युल्ड डिस्ट्रिक एक्ट 1874 के द्वारा ही छोटागनागपुर डिविजन के हजारीबाग, रॉंची, पलामू, मानभूम, परगना ढालभूम और सिंहभूम के कोल्हन क्षेत्र को भी शिड्युल्ड डिस्ट्रिक के रूप में घोषित किया गया था।
भारतीय शासन व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण, आदिवासी समाजों की विशिष्ट पहचान और सांस्कृति सम्पदा को बचाए रखने, उनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक हितों की रक्षा करने के लिए संविधान निर्माताओं ने देश के आदिवासी क्षेत्रों को दो हिस्सों में बॉंटा। Excluded and Partially Excluded Areas को अनुच्छेद 244 (1) (पॉंचवी अनुसूची) तथा अनुच्छेद 244 (2) छटवीं अनुसूची) (ट्रायबल क्षेत्र) के प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें स्वायतता प्रदान किया गया।
डुवार्स और तराई के अधिकतर आदिवासी चाय अंचलों में बसे हैं। उनकी बदहाली और विपन्नता किसी से छिपी नहीं हैं। वे रोजगार पर आधारित आय पर सम्पर्ण रूप से निर्भर हैं और इसी रोजगार के साधनों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करके आज आदिवासी समाज पर नियंत्रण रखा जा रहा है। उन्हें सीमित आय पर रहने के लिए मजबूर करके उनकी शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक और अन्य आर्थिक कार्यकलापों पर सीधा नियंत्रण रखा जा रहा है। एक आजाद देश में गुलाम जनता कैसी होती है, उसका यह एक जीता जागता उदाहरण है।
उनके कल्याण के लिए The Plantation Labour Act 1951 लागू किया गया है। लेकिन वह कागजों में सीमित है। डुवार्स तराई के 300 चाय बागानों में शायद ही कोई एक ऐसा बागान होगा, जिसमें टी प्लांटेशन एक्ट का उल्लंघन न किया गया होगा। इस उल्लंघन की बातों को सरकार से पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी रोज देखते हैं। सरकारी विभागों के श्रम इंस्पेक्टर और अन्य पदाधिकारी भी चाय बागानों में आकर इसे अपनी आंखों से देखते हैं। शायद वे अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख भी करते होंगे। लेकिन आज तक किसी बागान या प्रबंधन के विरूद्ध कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।
गरीब मजदूरों के वेतन से काटे गए प्रोविडेंट फंड के रूपयों को प्रोविडेंट फंड में जमा न करके उसके अरबों रूपयों को मालिक डकार गए लेकिन इप्लाइज प्रोविडेंड के रूपये के गबन में सिर्फ दिलासा देने की कार्रवाई की गई। जबकि रिटायरमेंट बेनेफिट्स के नाम से जमा होने वाले इस राशि के गबन करने के लिए न्यूनतम एफआईआर दायर करने, भारी आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान इसके लिए बने कानून में बनाया गया है। किसी भी चाय बागान में शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग से होने वाले प्रोफिट्स को अपने कर्मचारियों, मजदूरों के हित में खर्च करने के लिए कानून बने हुए हैं और इसके लिए टैक्स में छूट भी मिलता है। स्वास्थ्य सेवा की कमी से हर वर्ष कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। लेकिन राज्य में श्रम कानून को लागू करने वाले श्रम और सामान्य प्रशासनविभाग ने नियमित मौत के शिकार होते मजदूरों को भी देखकर अपनी ऑखें बंद किए बैठा है। ऐसा लगता है, विभाग का विवेक चाय बागानों की तरह ही बदहाल है। मजदूरों को नेतृत्व प्रदान करने का दावा करने वाले श्रमिक संघ हर बार न्यूनतम वेतन से कम में वेतन समझौता करके अपनी काबलियत का प्रदर्शन करते रहे हैं। वे कम बोनस देने पर भी निर्लज्जता पूर्वक प्रेस कांन्फ्रेस करके उसकी औचित्य बताते हैं।
पश्चिम बंगाल में आदिवासी जनता आजादी के बाद ही दोयम दर्जे का व्यवहार पाता रहा है। संविधान की पॉचवीं अनुसूची के अन्तर्गत 25 अगस्त 1953 को Tribal Advisory Council गठन किया गया था। लेकिन Tribal Advisory Council ने आदिवासी हित में क्या-क्या निर्णय लिया या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को क्या-क्या परामर्श दिया, यह आज तक आदिवासी जनता जान नहीं पाई है। पश्चिम बंगाल में Tribal Advisory Council तो बना दिया गया, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों को स्वशासन देने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया गया और किसी भी आदिवासी क्षेत्र को शिड्युल्ड एरिया घोषित नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ कि आदिवासी संस्कृति, भूमि, भाषा, समाज को शोषण से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया।
यदि आदिवासी क्षेत्रों को श्डियुल्ड एरिया घोषित किया जाता तो उनके हाल आज इतने खराब नहीं होते । लेकिन संविधान में विशेष उपबंध रहते हुए भी उन्हें सामान्य कानूनों के हवाले कर दिया गया और शोषण का चक्र अपनी गति से आज भी चल रहा है। ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा 14 मार्च 2012 को Tribal Advisory Council के विनियम में संशोघन जारी गया, लेकिन अभी आदिवासी समाज की क्लासिकल समस्याओं को लेकर यह कौंसिल ने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है, ऐसा कोई नाजिर अब तक नहीं मिला है। आदिवासी समाज के हित में काम करने वाले करीबन सभी संगठनों को इस बात का पता है लेकिन किसी भी संगठन ने अब तक इस बात को पुख्ता अंदाज में नहीं उठाया है। आदिवासी समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले पॉचवी अनुसूची के बदले वर्षो तक छटवीं अनुसूची की मांग करते रहे हैं। जब पाँचवीं अनुसूची ही लागू नहीं है और इसके सफल या असफल होने का कोई तथ्य, आंकड़ा या प्रभाव ही नहीं हुआ है तो इसे छोड़ कर कई संगठन छठवीं अनुसूची की मांग करते हैं। संविधान में उपयुक्त संशोधन के बिना कोई भी सरकार चाह कर भी छटवीं अनुसूची के उपबंधों को पश्चिम बंगाल के आदिवासी अंचलों में लागू नहीं कर सकती है।
पता नहीं किसने छटवीं अनुसूची का राग छेड कर इतना समय और उर्जा को अपव्यय करवाया और जनता को गलत ख्वाब दिखलाया। ऐसा लगता है चालाक लोगों ने पाँचवीं अनुसूची से ध्यान भटकाने के लिए छटवीं अनुसूची को कुछ लोगों के दिमाग में डाल दिया है और वे गुमराह हो गए। देश में कई राज्यों में छटवीं अनुसूची की मांग जरूर की जा रही है, लेकिन संवैधानिक रूप से उनके पास पाँचवी अनुसूची जैसे प्रावधान भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्राथमिक मांग के रूप में वे छटवीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं। जबकि पाँचवीं अनुसूची आदिवासियों के लिए पहले से ही संविधान में उपलब्ध है और इसे आसानी से लागू कराया जा सकता है। छठवीं अनुसूची की मांग करके आदिवासी संगठन गैर आदिवासियों के उस मांग का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें आदिवासी यानी एसटी घोषित करने की मांग की जा रही है। छठवीं अनुसूची वहीं लागू होता है, जिसे केन्द्र सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ट्राईबल एरिया घोषित करता है।
एक समय था जब आदिवासी समाज किसी का गुलाम नहीं था। लेकिन आज तो सभी लोग आदिवासी समाज को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। गैर आदिवासी तथा अपने स्वार्थ में लिप्त ताकतें तो आदिवासियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक और सामाजिक रूप से गुलाम बनाना ही चाहती हैं और बहुत हद तक वे कामयाब भी रहे हैं। वे आदिवासियों की जमीन को खरीदने, हड़पने के लिए केन्द्रिय रूप से फंड जमा करके उसे खरीदने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते हैं। लेकिन विडंबना की बात तो यह है कि अनेक आदिवासी भी अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आदिवासी समाज में ही जमीन दलालों की कोई कमी नहीं है। आज आदिवासियों के वोट, उनकी ताकत और एकता को अपने व्यक्तिगत व्यावसायों को सपोट करने, अपनी ठेकेदारी को मजबूती देने के लिए ही कई लोग आदिवासी समाज का नेता बनना चाहते हैं और कई लोग इसमें कामयाब भी हैं। ऐसे लोगों की दिली ख्वाहिसें हैं कि आदिवासी जनता उनके कदमों के नीचे ही रहे।
भारत के अनेक राज्यों में पॉंचवी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करके आदिवासी समाज को शोषण से बचाने के लिए संवैधानिक संरक्षा दी गई है। पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की दशा और दिशा अत्यंत शोचनीय है इसमें दो राय नहीं है। पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के कल्याणार्थ पॉंचवी अनुसूची के प्रावधानों के अन्तर्गत ट्राइबल एडवाजरी कौंसिल का गठन भी किया गया है। संविधान में राज्यपाल को आदिवासियों का संरक्षक कहा गया है। आदिवासी समाज में निरंतर बढ रहे शोषण और उससे उपजे असंतोष को दूर करने के लिए आदिवासी अंचलों में शिड्युल्ड एरिया बनाना आज समय की मांग है। जो आदिवासियों का सच्चा हितैषी होगा वह इस मांग से असहमत नहीं होगा।
1874 में आदिवासी जनता को शोषण और अन्याय से बचाने के लिए शिड्युल्ड डिस्ट्रिक बनाया गया था। लेकिन आज तो आदिवासियों की हालत सर्वाधिक शोषित और वंचित की है ऐसे में संविधान में उनके उपचार के लिए बनाए गए प्रावधान ही सच्चे रूप से आदिवासी जनता का उद्धार कर सकता है और यह उद्धार सिर्फ पॉंचवी अनुसूची को लागू करके ही हो सकता है। जब संविधान में संशोधन होगा, दूसरे क्षेत्रों में छटवीं अनुसूची लागू होगी तो उसका लाभ आदिवासी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल छटवीं अनूसूची के लिए समय, ऊर्जा, पैसा, उम्मीद को इसके लिए लगाना इसका अवव्यय ही है और इससे समाज का एक बड़ा ऊर्जा बेकार चला जाता है। आज के नेताओं की बौद्धिकता की कमी के कारण आज आजादी पसंद समाज दूसरे समाज का गुलाम बना हुआ है। इसमें परिवर्तन करने के लिए गंभीर चिंतन की जरूरत है। लेकिन इसे कौन करेगा? यही बड़ा सवाल है।


Share this content:



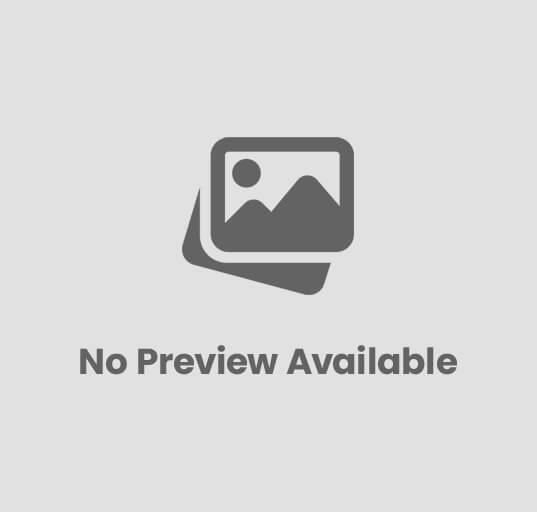


Post Comment