Interrelation of Spirituality With Religious Education and Religion आध्यात्मिकता का धार्मिक शिक्षा और धर्म से अंतरसंबंध
आध्यात्मिकता का धार्मिक शिक्षा और धर्म से अंतरसंबंध (Interrelation of spirituality with religious education and religion) एक महत्वपूर्ण विषय है। बालकों की वास्तविक शिक्षा और समाज में इस पर स्वास्थ्य चिंतन, मानवीय सभ्यता के संतुलित विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस पर पूर्णांग रूप से समझ पैदा करके ही कोई परिवार और समाज आगे बढ़ सकता है।

विभिन्न धाराओं से संचालित सामाजिक प्रथाओं और व्यवहारों के बरक्स व्यापक सामाजिक भागीदारी के लिए, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों के बीच मौजूद सूक्षम अंतरों के बारे पूर्णांग समझ रखना एक अपरिहार्य आवश्यकता बनते जा रही है।
अवार्चीन काल में समाज के भीतर मीडिया के सहारे साम्प्रदायिकता भरे नये नरेशन सृजित करने की कोशिशें जारी है। साम्प्रदायिकता और राजनैतिक झुकावों के ध्रुवीकरण के सहारे समग्र समाज को छिन्नभिन्न करने के प्रयास अपने आप में स्पष्ट हैं। पूरे समाज के चिंतन धारा को निरा धार्मिक सिद्धांतीकरण के रास्ते धकियाना एक खतरनाक खेल बन चुका है। नये बनने वाले नरेटिव स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रमुख बाड़ सिद्ध हो सकता है, जो वैश्विक स्तर पर बौद्धिकता के क्षरण और क्षुद्रता का प्रमुख कारण बन सकता है।
मीडिया, विशेष करके सोशल मीडिया तक व्यक्तिगत पहुँच के जमाने में, आप अपने परिवार के बच्चों को किन रास्तों पर धकेलना या प्रेरित करना चाहेंगे, यह आपके नैतिकता पूर्ण पूर्णांग धार्मिकता और आध्यात्मिकता की समझ पर निर्भर करता है। माता-पिता और समाज को तय करना होगा कि वे बच्चों को धार्मिक कट्टरता की ओर ले जाना चाहते हैं या उन्हें स्वतंत्र विचारधारा और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। परिवार और समाज में बच्चों को किस दिशा में बढ़ाया जाएगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि उनके अभिभावक धार्मिकता और आध्यात्मिकता के बीच के अंतर को कितनी गहराई से समझते हैं और उसे अपने बच्चों को किन पद्धतियों से उन्हें सौंपते हैं।
अभिभावकों के लिए अपने पारिवारिक परिधि से बाहर निकल कर, धर्म और आध्यात्मिकता के असली तत्वों तक दिमाग को ले जाना जरूरी हो गया है। क्यों और कैसे उसे जानना महत्वपूर्ण बन गया है। बिना सामुचित ज्ञान के मीडिया के गलत मार से बच्चों को बचाना और उन्हें सही रास्ते पर चिंतन के लिए प्रेरित करना बहुत मुश्किल कार्य हो गया है।
संगठित धर्मों का “आध्यात्मिकता का अध्येता” होने के दावे बहुत प्राचीन है। लेकिन तर्कवादियों का यह सवाल कि धर्म के साथ आध्यात्मिकता का रिश्ता, वास्तविक रूप में कितना प्रतिशत है? अपनी जगह पर हमेशा एक सवाल बन कर चुनौती देता रहा है। धार्मिक शिक्षा (Religious Education) और धर्म (Religion) का आध्यात्मिकता (Spirituality) से गहरा संबंध जरूर है। लेकिन धार्मिकता (Religiosity) और आध्यात्मिकता (Spirituality) एक समान नहीं हैं। इसमें जमीन असमान का अंतर है।
AMAZON.IN
Minimum 50% off Home, kitchen & more
Deals on accessories for your top smartphone brands
Purchase छूट के साथ खरीदें Click Here for Prices




इन्हें सही तरह से समझे बिना, कोई भी समाज या देश संतुलित विकास नहीं कर सकता। इनकी सतही समझ ने समाज और दुनिया में बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है। यह सार्वभौमिक यथार्थ है कि धर्म और आध्यात्मिकता न एक है और न एक समान हैं; बल्कि दोनों के बीच अंतरसंबंध होते हुए भी उनके बीच मीलों के फासलें हैं। उन्हें सही ढंग से समझे बिना न तो व्यक्ति का हित किया जा सकता है और न ही उसका सही उपयोग समाज के हित में किया जा सकता है।
समाज में धार्मिकता और आध्यात्मिकता के बीच स्पष्ट और निर्णायक समझ विकसित करके ही मानव कल्याण के लिए सही दिशा में प्रगति की जा सकती है। यदि यह समझ अधूरी हो, तो इससे असंतुलन पैदा हो सकता है, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर इसका वास्तविक रूप से कोई लाभ नहीं होगा। दुनिया की अधिकतर समस्याओं के पीछे इस समझ की कमी अपने आप स्पष्ट है।
.
धर्म और आध्यात्मिकता दोनों की आवधारणाएं विलग है। इस पर तार्किकता से भरे प्राचीन और अवार्चीन साहित्य उपलब्ध हैं। नास्तिक तार्किक आंदोलन ने इस पर गंभीर चिंतन करके इसके पारंपारिक विचारों को तार्किकता से नये रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। धार्मिक किताबें आध्यात्मिकता के लिए एक विकसित दुनिया प्रदान करने का दावा करता रहा है। उसे वह अपने विशेष धर्म के ऊपर अवलंबित होने की सूचना देता रहा है।
लेकिन आध्यात्मिकता संगठित धर्म से स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग मौजूद हो सकता है। दुनिया के अधिकतर प्राचीन और अवार्चीन दार्शनिकों ने आध्यात्मिकता की राह को सामाजिक या सांस्कृतिक से सने हुए धर्म से बिल्कुल अलग एक स्वतंत्रता पथ माना है। आध्यात्मिकता की राह में चलने, उसे अपनाने और उसका अभ्यास करने के लिए संगठित धर्म के अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती है।
संगठित धर्म मूर्त सार्वजनिक दिखाऊटी कर्मकांडों का एक समुच्च्य होता है। कई रूढ़ प्रार्थनाओं, आराधनाओं, नियम कायदों, ऊँच-नीच वर्ग या समुदाय (पुजारी-गैर पुजारी वर्ग), रूपये पैसों, रूढ धार्मिक प्रतीक इसके अभिन्न अंग होते हैं। इसके बाहर संगठित धर्मों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हर धर्म का अपना एक परिचय और मूर्त अस्तित्व होता है।
दुनिया के अधिकतर धर्म का अपना अदृयमान विशिष्ट विशेषताओं वाला ईश्वर या परम ईश्वर अवश्य होता है। विशिष्ट चारित्रिक विशेषताओं से मुक्त किसी भी संगठित धर्म का कोई देवता, ईश्वर या परम ईश्वर नहीं होता है, इसका एक अर्थ यह है कि सभी धर्मों के देवता और ईश्वरों का एक अलग पहचान और अस्तित्व होता है। पारंपारिक धर्म के अस्तित्व के लिए विशिष्ट कार्य करने वाला अलग ईश्वर का होना एक अनिवार्य तत्व होता है। प्रत्येक धर्म के अंदर इसी ईश्वर या देवता या परम शक्ति को आध्यात्मिकता का परम स्रोत या बिन्दु माना गया है।
दूसरे शब्दों में कहें तो अपने ईश्वर सहित प्रत्येक धर्म एक विशिष्ट सम्प्रदाय और साम्प्रदायिकता का निर्माण करता है। उस ईश्वर या देवता को मानने वाले एक विशिष्ट पहचान के साथ अलग धार्मिक या सम्प्रदायिक समूह होता है। जो व्यक्ति उक्त धर्म विशेष के ईश्वर पर आस्था नहीं रखता है। वह उस धर्म के लिए बाहरी व्यक्ति होता है। अर्थात् एक धर्म के ईश्वर एक विशेष साम्प्रदायिक समूह का निर्माण करता है और वह दूसरे सम्प्रदायिक समूह के लिए बेगाना होता है। यहाँ विशेष ईश्वर पर आस्था रखने वाले, अपने विश्वास और खास नियमों के तहत, दूसरे समूह से अपने को अलग मानता है और वह वृहत्तर मानवीय समाज से अपने समाज को भी अलग मानता है। वह अपने धर्म समूह के लिए एक कुकून का निर्माण करता है, जिसमें दूसरे समूह के इंसान प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
.
धर्म का मुख्य कार्य आध्यात्मिकता से इतर होता है। वह सांस्कृतिक प्रतीकों और रूपये पैसों के इर्द गिर्द कार्यकलाप करता है। धर्म और आध्यात्मिकता का अस्तित्व ही अलग-अलग होता है। धर्म अपने अनुयायियों से हमेशा आध्यात्मिकता के नाम पर अपने से जुड़े रहने का आग्रह करता है।
जबकि आध्यात्मिकता के लिए सिर्फ जन के मन की आवश्यकता होती है, विशिष्ट साम्प्रदायिक भावनाओं से संचित धार्मिक समूह वाला एकताबद्ध जनसंख्या की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आध्यात्मिकता का संसार दिल और दिमाग के अंदर होता है और उसे बाहरी सांस्कृतिक कर्मकांडों या पहचान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आध्यात्मिकता का कोई सम्प्रदाय नहीं होता है और न ही कोई कर्मकांड वाला ईश्वर या देवता।
हालांकि धर्म समूह को अपने तथाकथित आध्यात्मिकता को बचाए रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मकांडी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक वर्चस्व के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भारी भीड़ और विशाल जनसंख्या के साथ रूपये पैसे की आवश्यकता होती है। यही वह बिन्दु है जो आध्यात्मिकता से धर्म को अलग-थलग करता है। सांस्कृतिक धर्म सिर्फ आध्यात्मिकता के सहारे जिंदा नहीं रह सकता है, बल्कि उसे जिंदा रहने के लिए एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भीड़, कर्मकांड, रूपये पैसे और एक सम्प्रदायिक पहचान दिलाने वाला दल की आवश्यकता होती है।
.
बिना विशाल जनसंख्या के कोई भी संगठित धर्म का स्वतंत्र आर्थिक वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाता है। धर्मांतरण या घर वापसी, प्राण प्रतिष्ठा, धार्मिक मेला, यात्रा, धार्मिक दंगों के में निर्लिप्तता, विशिष्ट आर्थिक और राजनैतिक हित लक्ष्य, रणनीति, कूटनीति और धार्मिक रणनीतियों और लड़ाईयों को इसके बरक्स समझा जा सकता है।
मूर्त और शुद्ध कर्मकांडी धर्मों को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आर्थिक ढाँचागत वर्चस्व को स्थायी रूप से बनाए रखना होता है। यह आश्चर्चजनक रूप से वैश्विक रूप में एकरूपता लिए सभी जगह हाजिर रहा है। यही आर्थिक व्यवस्था ही धर्म के पुजारी वर्ग (भारत के संबंध में इसे पुजारी वर्ण समुदाय पढ़ा जाए) के अस्तित्व को बनाए रखने का पूँजीवादी सम्पदा एकत्रित करने की पद्धति है। इसे समझे बिना आप धर्म के पूँजीवादी स्वरूप को पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं। इस धार्मिक आर्थिक सम्पदा के बगैर मूर्त कर्मकांडी धर्म का कोई स्वतंत्र और प्रभावशाली अस्तित्व नहीं होता है। धर्म के कर्मकांडों का रूपये पैसे से प्रगाढ़ संबंध होता है। बिना पैसे के कोई भी धर्म जीवित नहीं रह सकता है। अधिकतर धर्म का मुख्य लक्ष्य विशाल धन सम्पदा एकत्र करना होता है और इसके माध्यम से वे जनता के बीच अपनी राजसत्ता कायम करते हैं। वर्तमान में धार्मिक धन सम्पदा राजनीति को साधने और सत्ता हथियाने का उपकरण बन गया है। यही वह बिन्दु है जो धर्म और धार्मिकता को पूँजीवादी व्यवस्था का अभिन्न अंग सिद्ध करता है। गैर पूँजीवादी व्यवस्था में धर्म का जीवित रहना संभव नहीं है। साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था में धर्म धन सम्पदा एकत्र करके आर्थिक जमींदारी स्थापित नहीं कर पाता है, इसीलिए धर्म का पसंदीदा राजसत्ता पूँजीवादी राजसत्ता होता है।
.
धार्मिक संस्थाओं के प्रतीक पूजा और आराधना स्थलों को प्राचीन काल से ही अत्यंत विशाल और भव्य बनाए रखने की परंपरा को इसकी मानसिकता और मनोवैज्ञानिकता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विशालता, विशाल मानवीय समूह का जुटान, भव्यता ग्लैमर्स के जादुई शक्ति से हर युग में जनता बहुत प्रभावित रही है। इन बातों से मीडिया के माध्यम से एक विशिष्ट नरेटिव का निर्माण होता है तो आम जनता को मंत्रमुग्ध करता है। उसमें मनोवैज्ञानिक अपील का निर्माण करता है। इन तमाम धार्मिक कार्यकलापों के पीछे जनसंख्या की मानसिक चिंतन को अपने अधीन बनाए रखना, धन कमाना और उसके माध्यम से सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य छिपा रहता है।
भव्यता के भव्य प्रभाव से तर्कहीन जनता को प्रभावित करने के लिए कल्पित कथा कहानियाँ, उत्सव उमंग वगैरह डालने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इसमें धार्मिक मार्केटिंग का अनुसांगिक तत्व अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं।
वैज्ञानिकता से अन्जान तर्कहीन दिमागों में विशेष मार्केटिंग के द्वारा धार्मिक श्रद्धा और भक्ति भरे जाते हैं। इसके लिए हर युग में उपलब्ध मीडिया का प्रयोग राजकीय धन से करने के ऐतिहासिक विवरण विश्व इतिहास में भरे हुए हैं। धार्मिक वर्चस्व पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास और पूँजी के समेकन (Consolidation of capital) के इर्दगिर्द चक्कर काटते कर्मकांडों में कही कोई आध्यात्मिकता नहीं होता है। आर्थिक और राजनैतिक लक्ष्यों को लेकर होने वाले कार्यकलापों में आध्यत्मिकता का कोई स्थान नहीं होता है। भले धार्मिक लोगों के मेकअप और बोली वचनों में धार्मिक शब्दों का घालमेल हो। यह ठीक है कि कई व्यक्ति पारंपरिक धार्मिक संस्थानों के कर्मकांडों में लिप्त होकर भी आध्यात्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अपनाते हैं। लेकिन इसका प्रतिशत कितना है? यह सवाल हमेशा प्रसांगिक रहा है।
.
धार्मिक वर्चस्ववादी अर्थव्यवस्था और इसके दूरगामी प्रभावी ढांचा को मजबूत करने के लिए धार्मिक मार्केटिंग को कई हिस्सों में बाँटा जाता है। सबसे पहले इसके लिए बच्चों और अनपढ़ जनता, विशेष कर घरेलू, पारंपारिक, तर्कहीन, घरेलू महिलाओं और तर्किता से दूर आम पुरूषों को प्रथम टारगेर वर्ग बनाया जाता है। इसके लिए यदि कर्मकांडी शासकों के हाथों में कानून बनाने की शक्ति होती है तो वह धर्म के कर्मकांडी भाग को प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाता है और बाल शिक्षा के रास्ते मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए रास्ते अपनाए जाते हैं। इसके अलावा भी सत्ता के बल पर धार्मिक कर्मकांडों पर रूपये पैसे खर्च करके नये कीर्तिमान भरे धार्मिक रिकार्ड बनाए जाते हैं और जिसे धर्म के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष के रूप में प्रचारित किया जाता है।
.
बहुमुखीहीन एकांगी शिक्षा वैकाल्पिक समतामूलक मान्यताओं को विद्यार्थी दिमाग में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। बालकों के मन में स्वतंत्र वैश्विक विविधतापूर्ण जीवन शैली और दर्शन को आत्मसात करने और समझने में बाधाएँ डालने के लिए नियोजित पद्धति अपनाई जाती है। यदि लगातार दो तीन पीढ़ियों तक बालकों को शिक्षा के माध्यम से एकांगी दर्शन और जीवन मूल्यों को दिमाग में ठूँसा जाता है, तो वहाँ वैकाल्पिक जीवन दर्शन के प्रवेश का हर रास्ता बंद हो जाता है। कई कट्टर ईसाई और कठमूल्लापूर्ण मुस्लिम देशों के शिक्षा पाठ्यक्रमों और उसके प्रभाव पर रिसर्च करके इसे पूर्णांग रूप से समझा जा सकता है। क्यों मुस्लिम देशों में धार्मिक सहजीवन के लिए कोई आदर्श अनुकूल वातावरण नहीं है, इसे बालकों को दी जाने वाली सार्वजनिक शिक्षा के रास्ते धार्मिक सिद्धांतकारी योजना से भी समझा जा सकता है। भारत में कट्टर धार्मिक शिक्षा देने के लिए आदिवासी और पिछड़े इलाकों में हिन्दू माईथोल़ॉजी के किताबों को नियोजित ढंग से पढ़ाने के लिए योजनाएँ बनाने और उसका कार्यान्वयन करने की कई खबरें आम हुई है, ताकि साम्प्रदायिक भावनाओं से रहित बालकों के मन में एक विशेष धर्म के प्रति एकांगी धार्मिक कट्टरता की भावनाएं भरी जा सकें।
.
धार्मिक शिक्षा का आदर्शवादी उद्देश्य, आदर्श रूप से, बच्चों को बेहतर जीवन जीने और उनके समुदायों में सकारात्मक योगदान देने में मदद करना है, लेकिन यह स्वतंत्र और सीमाहीन अनुकूलनशीलता या चिंतन की लचकता को सीमित कर देता है। लंबे समय तक चलने वाले अध्ययनों से पता चलता है कि स्कूलों में साम्यवादी या धार्मिक शिक्षा या साम्प्रदायिक शिक्षा से विविधता पूर्ण चिंतन प्रक्रिया पर लगाम कस जाती है। ऐसी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का चिंतन और व्यवहार कट्टर साम्प्रदायिक वाला बन जाता है। इससे सभ्यता के संतुलित समग्र विकास के लिए शिक्षा के रास्ते में मानव पूंजी निवेश पूरी तरह प्रभावित हो जाता है।
.
यदि मानव समाज को धर्म की कोई आवश्यकता है, तो उससे भी अधिक आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। यह कर्मकांडी नहीं होता है। यह साम्प्रदायिक भी नहीं होता है। कर्मकांडी प्रभावित शासक और शासन आध्यात्मिकता का विरोधी हो सकता है। यह सर्वधर्म और विविधता का विरोधी भी हो सकता है। इसलिए बच्चों को आंखें बंद करके धार्मिक वर्चस्व के लिए चलाए जा रहे मुहिम से बचाया जाना चाहिए। उनके मन में एक कर्मकांड के लिए अनुराग और दूसरे के लिए विराग उत्पन्न होने के बचाने का प्रथम कर्तव्य माँ-बाप और परिवार और समाज का होता है। उन्हें यह कर्तव्य हमेशा याद रखना चाहिए। यदि साम्प्रदायिकता की भावना रहित सच्चा आध्यात्मिकता की शिक्षा बच्चों को दिया जाए, तो बच्चों का दिमाग एकांगी सोच का शिकार नहीं होगा और वह सार्वभौमिक हित के लिए चिंतन मनन करने वाला एक निष्पक्ष रचनात्मक सृजनशील व्यक्ति होगा, जो परिवार और समाज के लिए एक अमूल्य सम्पदा होगा। नेहइंद।
Share this content:
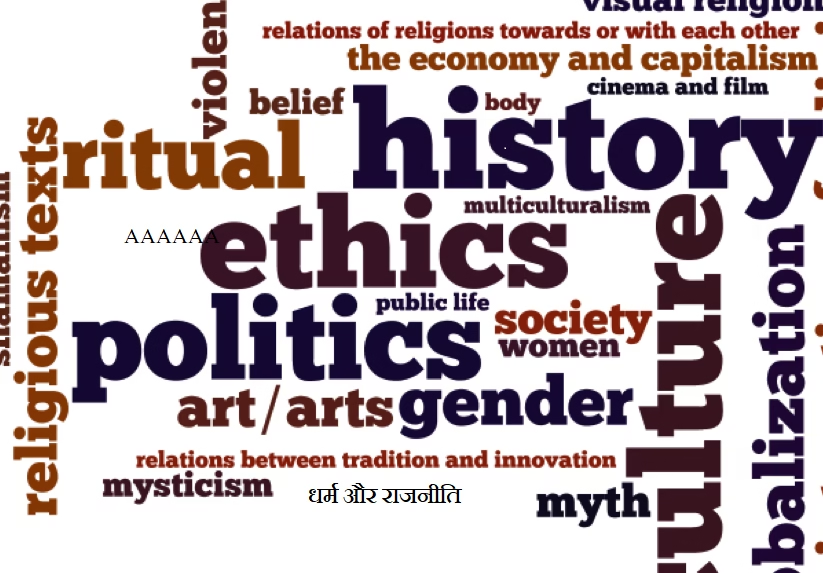


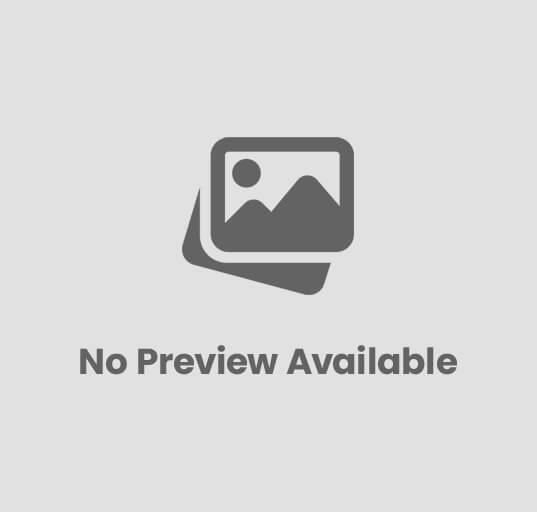


Post Comment